UPSC के लिए प्रासंगिकता
● GS पेपर II (शासन): एआई नीति, नियमन और समावेशिता
● GS पेपर III (अर्थव्यवस्था और तकनीक): एआई का रोजगार, उत्पादकता और एमएसएमई पर प्रभाव
● निबंध: “कृत्रिम बुद्धिमत्ता: विकास में एक साझेदार, न कि आजीविका के लिए खतरा”
समाचार में क्यों?
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial intelligence) दुनियाभर में उत्पादकता और नवाचार का एक प्रमुख स्रोत बनती जा रही है। भारत में इसे एक ऐसा अवसर माना जा रहा है जिससे लाखों नौकरियाँ पैदा हो सकती हैं, लेकिन साथ ही यह एक चुनौती भी है क्योंकि इससे मौजूदा नौकरियाँ खत्म होने का खतरा भी है।
● ServiceNow–Pearson AI Skills Research 2025 रिपोर्ट के अनुसार, एआई लगभग 1.035 करोड़ नौकरियों की रूप रेखा को बदल सकता है और 2030 तक 30 लाख नई तकनीकी नौकरियाँ पैदा कर सकता है।
● यह भारत को एआई के जरिए बदलाव लाने के मामले में सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया से आगे रखता है।
● हालांकि, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने चेतावनी दी है कि जहाँ नए काम सामने आएंगे, वहीं कई पुराने काम खासकर श्रम-आधारित क्षेत्रों में, खत्म भी हो सकते हैं।
इसलिए, भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है: एआई को कैसे ऐसा बनाया जाए कि वह लोगों, एमएसएमई(MSME) और छोटे उद्यमियों को सहयोग करे, न कि उनकी जगह ले?
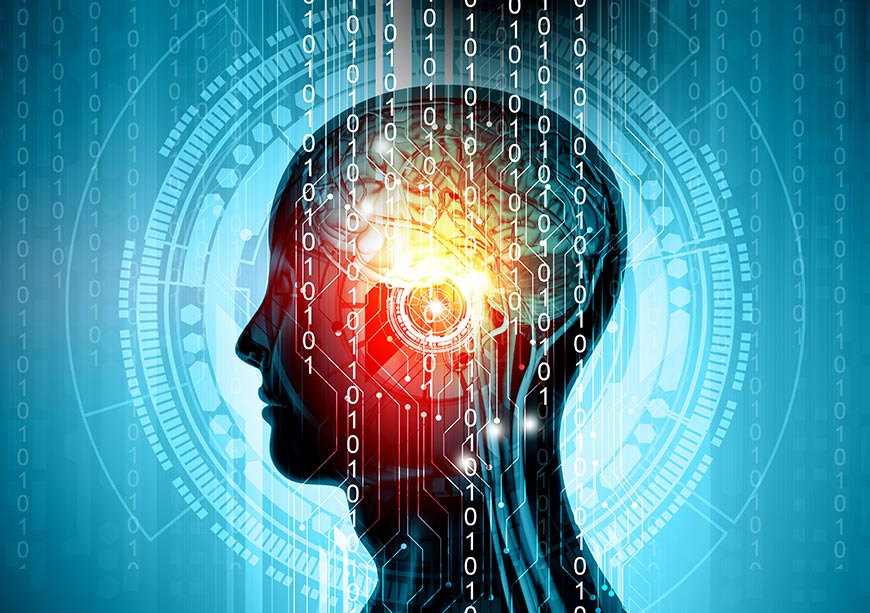
पृष्ठभूमि: भारत की रोजगार संरचना और एआई की दुविधा
भारत की अर्थव्यवस्था श्रम-आधारित है। यहाँ कृषि और कम-कुशल सेवाओं में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। लेकिन इन क्षेत्रों में अभी तक एआई का बहुत कम उपयोग हुआ है।
● श्रम-प्रधान सेवाएँ: ये सेवाएँ भारत की जीडीपी में 55% योगदान देती हैं और कुल नौकरियों में 31% (FY24) हिस्सा रखती हैं। इसमें खुदरा (रिटेल), होटल और रेस्टोरेंट, लॉजिस्टिक्स और आईटी सेवाएँ शामिल हैं।
● कृषि: यह अब भी यह भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता (रोजगार देने वाला क्षेत्र) है, लेकिन एआई को अपनाने में यह तकनीकी रूप से काफी पीछे है।
एआई की दुविधा:
1. स्वचालन (Automation) के तहत —AI का उपयोग करके कर्मचारियों को हटाना और कामकाज को अधिक कुशल बनाना।
○ उदाहरण: बैंकों द्वारा एआई चैटबॉट्स (AI chatbots) का इस्तेमाल करना, जो इंसानी कस्टमर सपोर्ट की जगह ले रही हैं।
○ जोखिम: रूटीन (हर रोज़ के) काम करने वाले कर्मचारियों की बड़ी संख्या में नौकरियाँ जा सकती हैं।
2. सहयोगात्मक रूप से (Augmentation Path) —
- AI का इस्तेमाल मानव कर्मचारियों की मदद के लिए करना, ताकि उनकी उत्पादकता बढ़े और नौकरियाँ बनी रहें।
○ उदाहरण: डॉक्टरों द्वारा बीमारियाँ जल्दी पहचानने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल करना।
○ फायदा: कर्मचारी की आवश्यकता बनी रहती हैं और काम की रफ्तार भी बढ़ती है।
नीति से जुड़ा सवाल:
क्या भारत एआई को एक साथी (साथ काम करने वाला) के रूप में अपनाएगा या एक विनाशक (नौकरियाँ खत्म करने वाला) के रूप में?
भारत में एआई अपनाने की चुनौतियाँ
1. धीमी गति से कौशल विकास और दोबारा प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत:
○ कर्मचारी एआई से जुड़े नए कामों के लिए जल्दी से खुद को तैयार नहीं कर पा रहे हैं।
○ भारत में व्यावसायिक (हुनर आधारित) प्रशिक्षण सीमित है, और जीवन भर सीखते रहने की व्यवस्था कमजोर है।
○ उदाहरण: Infosys ने इंजीनियरों के लिए दोबारा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन छोटे शहरों के कर्मचारियों को अब भी एआई प्रशिक्षण की सुविधा नहीं मिल रही है।
2. श्रमबल में भारी असंगठितता
○ भारत के लगभग 80–85% कर्मचारी असंगठित क्षेत्र में हैं।
○ असंगठित कर्मचारियों के पास सामाजिक सुरक्षा नहीं होती, इसलिए अगर एआई के कारण नौकरियों की मांग घटती है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे।
3. कुछ क्षेत्रों की ज़्यादा संवेदनशीलता
○ रिटेल, बीपीओ और लॉजिस्टिक्स जैसी श्रम-प्रधान सेवाएँ एआई से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकती हैं।
○ उदाहरण: कॉल सेंटर में काम करने वाले लोगों की जगह जनरेटिव एआई वॉइस बॉट्स ले सकते हैं।
4. डिजिटल खाई (Digital Divide)
○ छोटे व्यवसायों (MSMEs) के पास क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई सॉफ्टवेयर या डिजिटल टूल्स के लिए पैसा नहीं होता।
○ इससे खतरा है कि बड़ी कंपनियाँ एआई का पूरा फायदा उठा लेंगी और छोटे कारोबार पीछे छूट जाएंगे।
- 5. शक्ति का केंद्रीकरण (Concentration of Power)
○ एआई से जुडी ज़रूरी चीज़ें — जैसे क्लाउड स्टोरेज, बड़ी एआई मॉडल्स और भारी कंप्यूटिंग — कुछ गिनी-चुनी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ ही चला सकती हैं।
○ उदाहरण: अगर Google, Microsoft या OpenAI जैसी कंपनियाँ एआई प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण रखती हैं, तो भारतीय स्टार्टअप्स को टक्कर देना मुश्किल हो सकता है।
भारत के लिए एआई के अवसर
जोखिमों के बावजूद, अगर सही दिशा में इसका उपयोग किया जाए तो एआई भारत के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है जैसे:
1. उत्पादकता बढ़ावा देने के रूप में:
○ कृषि में एआई: प्रीसिजन फार्मिंग टूल्स की मदद से किसान मिट्टी, पानी और फसल की सेहत पर नज़र रख सकते हैं।
○ स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई: बीमारियों की शुरुआती पहचान एआई इमेजिंग से संभव हो सकती है।
○ लॉजिस्टिक्स में एआई: सामान की डिलीवरी का समय और लागत कम की जा सकती है।
2. जीवनभर सीखने और कौशल विकास को बढ़ावा देने में:
○ स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में एआई से जुड़ा प्रशिक्षण शामिल करना।
○ उदाहरण: Future Skills PRIME और Startup India जैसे कार्यक्रम पहले से ही युवाओं को डिजिटल नौकरियों के लिए तैयार कर रहे हैं।
3. एमएसएमई (MSME) को सशक्त बनाने में:
○ जनरेटिव एआई टूल्स (जैसे चैटबॉट्स, कम लागत वाले डिज़ाइन सॉफ्टवेयर) छोटे कारोबारों को बड़ी कंपनियों से मुकाबला करने में मदद कर सकते हैं।
○ उदाहरण: एक हस्तशिल्प विक्रेता एआई-आधारित ई-कॉमर्स एनालिटिक्स की मदद से अपने ग्राहकों तक बेहतर पहुँच बना सकता है।
4. नवाचार और उद्यमिता (Entrepreneurship)
○ fintech, ed-tech, and agri-tech जैसे क्षेत्रों में एआई स्टार्टअप्स उभर रहे हैं।
○ उदाहरण: एआई आधारित प्लेटफ़ॉर्म किसानों को मौसम और बाज़ार की कीमतों की जानकारी रियल-टाइम में दे रहे हैं।
सरकार और नीतियों की भूमिका
अगर भारत चाहता है कि एआई एक सहायक (enabler) बने, तो इसके लिए मजबूत नीति-निर्माण ज़रूरी है:
1. एआई के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) बनाना
● जैसे UPI ने भुगतान (payments) की दुनिया बदल दी, वैसे ही भारत को एआई के लिए खुले डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बनाने होंगे।
● इसकी प्रमुख विशेषताएँ:
○ साझा डेटा सेट्स को सार्वजनिक संसाधन (public goods) के रूप में उपलब्ध कराना।
○ कंप्यूटिंग ताकत (computing power) तक सस्ता और आसान पहुंच को बनाना।
2. एआई नवाचार को लोकतांत्रिक बनाना (Democratising AI Innovation)
● भारतीय भाषाओं और जरूरतों के अनुसार छोटे भाषा मॉडल (SLMs) तैयार करना।
● ऐसे AI टूल्स को बढ़ावा देना जो क्षेत्रीय भाषाओं में काम करें, ताकि एआई सिर्फ अंग्रेज़ी जानने वालों तक सीमित न रहे।
● उदाहरण: किसानों के लिए हिंदी या तमिल में मौसम की जानकारी देने वाला एआई मॉडल।
3. समावेशी कौशल विकास और श्रमिक सुरक्षा
● कम और ज्यादा कुशल सभी प्रकार के कामगारों के लिए एक राष्ट्रीय एआई कौशल मिशन शुरू करना।
● एआई को सामाजिक सुरक्षा (जैसे बेरोजगारी बीमा) से जोड़ना।
● यह सुनिश्चित करना कि एआई सिर्फ लागत घटाने के लिए नहीं, बल्कि श्रमिकों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो।
4. एमएसएमई-केन्द्रित एआई अपनाना
● छोटे व्यवसायों को सस्ती क्लाउड सेवा देना।
● एआई स्टार्टअप्स के लिए इनक्यूबेटर, एक्सेलेरेटर और मेंटरिंग सेंटर बनाना।
● छोटे कारोबारों को एआई अपनाने में आर्थिक सहायता (सब्सिडी) देना।
आगे की राह
● डेटा और कंप्यूटिंग को सार्वजनिक संसाधन माना जाए: ऐसा करने से कुछ बड़ी कंपनियों के हाथों इनका एकाधिकार (monopoly) नहीं होगा।
● स्वदेशी विकास को बढ़ावा दें: भारत की ज़रूरतों के अनुसार एआई मॉडल और स्टार्टअप्स में निवेश करें।
● सार्वजनिक-निजी भागीदारी: कौशल विकास और नवाचार के लिए उद्योग, शिक्षा संस्थानों और सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा दें।
● समावेशी विकास: यह सुनिश्चित करें कि एआई का लाभ किसानों, असंगठित श्रमिकों और छोटे व्यापारों तक पहुँचे — न कि केवल बड़ी कंपनियों तक।
● कुशलता और रोजगार में संतुलन बनाएँ: जहाँ संभव हो, वहाँ एआई का उपयोग मानव श्रम का सहयोग करने के लिए करें, न कि उसे हटाने के लिए।
निष्कर्ष
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) भारत के सामने एक ऐतिहासिक विकल्प प्रस्तुत करती है। यह या तो कमज़ोर श्रमिकों की नौकरियाँ छीनकर असमानता बढ़ा सकती है, या फिर एमएसएमई को सशक्त बनाकर और उत्पादकता बढ़ाकर एक समान अवसर देने वाला साधन बन सकती है।
👉 सही नीतियों, डिजिटल ढाँचे, समावेशी कौशल विकास और श्रमिक सुरक्षा के साथ, भारत एआई को आजीविका को बाधित करने वाला नहीं, बल्कि समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाला साधन बना सकता है।
प्रश्न 1: भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- एआई में स्वचालन (Automation) का उद्देश्य मानव श्रमिकों की जगह लेकर दक्षता बढ़ाना है, जबकि पूरकता (Augmentation) मानव श्रम के साथ मिलकर काम करती है।
- श्रम-प्रधान सेवाएँ भारत की GDP में 50% से अधिक योगदान देती हैं और लगभग 30% लोगों को रोजगार देती हैं।
- भारत ने पहले ही बड़े स्तर पर स्वदेशी (indigenous) एआई मॉडल विकसित और लागू कर लिए हैं, जो वैश्विक कंपनियों के समकक्ष हैं।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
A. 1 और 2 केवल
B. 2 और 3 केवल
C. 1 और 3 केवल
D. 1, 2 और 3
उत्तर: A
(स्पष्टीकरण: भारत अभी स्वदेशी बड़े एआई मॉडल विकसित करने की प्रक्रिया में है, लेकिन वैश्विक कंपनियाँ जैसे OpenAI, Google अभी भी हावी हैं।)
प्रश्न 2: निम्न में से कौन-से विकल्प भारत के एआई के लिए डिजिटल सार्वजनिक ढाँचे (Digital Public Infrastructure – DPI) का हिस्सा माने जा सकते हैं?
- ओपन एपीआई (Open APIs)
- सार्वजनिक डेटा सेट (Public datasets) को साझा संसाधन के रूप में
- क्लाउड और कंप्यूटिंग पावर तक सस्ती पहुँच
- बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित निजी मॉडल (Proprietary Models)
सही उत्तर का चयन करें:
A. 1, 2 और 3 केवल
B. 2 और 4 केवल
C. 1, 3 और 4 केवल
D. 1, 2, 3 और 4
उत्तर: A
(स्पष्टीकरण: चौथा विकल्प — निजी मॉडल जो सिर्फ बड़ी कंपनियाँ चलाती हैं — सार्वजनिक ढाँचे के सिद्धांतों के खिलाफ है।)
प्रश्न 3: निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:
| कार्यक्रम / पहल | केंद्रित क्षेत्र |
| 1. Future Skills PRIME | युवाओं के लिए डिजिटल कौशल विकास |
| 2. Startup India | नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना |
| 3. UNNATI | एआई और उन्नत तकनीकों में पुनः कौशल विकास |
उपरोक्त में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं?
A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3 सभी
उत्तर: D
(तीनों कार्यक्रम डिजिटल अर्थव्यवस्था और एआई से जुड़े मानव संसाधन विकास पर केंद्रित हैं।)
UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न:
“यदि नीतियाँ ‘सहयोग’ और ‘नवाचार के लोकतंत्रीकरण’ पर केंद्रित हों, तो एआई भारत का ‘साथी’ बन सकता है, ‘विनाशक’ नहीं।” भारत की रोजगार संरचना और डिजिटल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इस कथन की विवेचना करें।
(15 अंक, 250 शब्द)
स्रोत — द इंडियन एक्सप्रेस
क्या आपको लाभदायक लगा?
पुनरावृत्ति के लिए बुकमार्क करें, मुख्य परीक्षा का अभ्यास करें, और इसे अपने साथी अभ्यर्थियों के साथ साझा करें! धन्यवाद
