UPSC प्रासंगिकता – मेन्स:
- GS पेपर II (राजनीति और संविधान): भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न संविधानिक विचारधाराओं की जांच करें।
- निबंध पत्र: “भारत का संविधानिक आत्मा: बहुसंख्यक आदर्शों का प्रतिबिंब”।
चर्चा में क्यों है?
भारत अपनी लोकतांत्रिक गणराज्य के सात दशकों से अधिक का जश्न मना रहा है, और इस बीच 1950 से पहले के भारत के संविधानिक दृष्टिकोण पर बढ़ती अकादमिक रुचि देखी जा रही है। 1895 से 1948 के बीच, राष्ट्रीय विचारकों द्वारा विभिन्न संविधान मसौदों का प्रस्ताव किया गया था — प्रत्येक ने शासन, संप्रभुता और नागरिकता के अद्वितीय वैचारिक मॉडल का प्रतिनिधित्व किया।
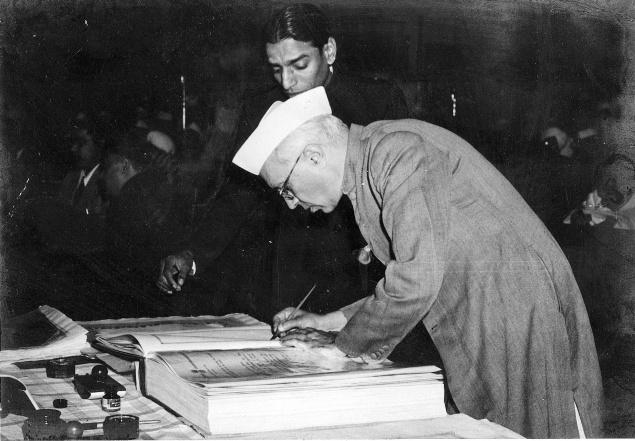
पृष्ठभूमि: भारतीय संविधान के पूर्ववर्ती विचारधाराएँ
1950 का भारतीय संविधान ‘संविधान सभा’ के भीतर गहन विचार-विमर्श का परिणाम था। हालांकि, इससे पहले कई नेताओं और राजनीतिक संगठनों ने अपने-अपने संविधान के मसौदे तैयार किए थे।
इन प्रारंभिक संविधान प्रस्तावों ने विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं को प्रदर्शित किया, जिनमें शामिल थे:
- उदारवाद
- रैडिकल मानवतावाद
- गांधीवादी विकेंद्रीकरण
- दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद
- समाजवादी लोकतंत्र
➡️ ये वैचारिक धाराएँ स्वतंत्रता के बाद अपनाए गए संविधान की बहुलवादी और समावेशी प्रकृति की नींव रखती हैं।
प्रारंभिक संवैधानिक उदारवाद: भारतीय संविधान बिल, 1895
भारतीय संविधान बिल, 1895 भारतीय नेताओं द्वारा ब्रिटिश शासन के तहत स्व-शासन की कल्पना करने का एक प्रमुख और प्रारंभिक प्रयास था। इसे शुरुआती राष्ट्रीयतावादियों जैसे बाल गंगाधर तिलक ने तैयार किया था, और इसका उद्देश्य ब्रिटिश प्रणाली के समान भारत के लिए एक संविधानिक ढांचा प्रस्तुत करना था, हालांकि यह पूर्ण स्वतंत्रता की बजाय डोमिनियन स्टेटस (स्वशासन) की मांग करता था।
मुख्य विशेषताएँ:
- इसमें 110 अनुच्छेद थे – उस समय के लिए यह एक विस्तृत दस्तावेज़ था
- ब्रिटिश संविधानवाद से प्रेरित
- नागरिक स्वतंत्रताओं पर विशेष जोर, जिसमें शामिल थे:
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- संपत्ति का अधिकार
- कानून के समक्ष समानता
- एक प्रतिनिधि शासन की आवश्यकता जताई गई।
- विधायिका, कार्यपालिका, और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण प्रस्तावित किया गया।
- ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करने का उद्देश्य, पूर्ण संप्रभुता की वकालत नहीं।
रैडिकल मानवतावाद और सहभागी लोकतंत्र: एम.एन. रॉय का 1944 मसौदा
1944 में, एम.एन. रॉय, एक क्रांतिकारी विचारक और रैडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक ने “स्वतंत्र भारत का संविधान: एक मसौदा” नामक एक दूरदर्शी संविधानिक प्रस्ताव तैयार किया। रैडिकल मानवतावाद में निहित, रॉय के मसौदे ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सहभागी लोकतंत्र, और विकेन्द्रीकृत शासन पर जोर दिया—यह मॉडल उपनिवेशी शासन और पारंपरिक संसदीय प्रणालियों दोनों को चुनौती देता था।
विशिष्ट विशेषताएँ:
- लोकप्रिय संप्रभुता और भाषाई संघवाद का समर्थन किया
- शहरी स्तर पर नागरिकों की समितियों का प्रस्ताव किया, ताकि शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित हो सके
- नागरिक-राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को भी कवर करते हुए एक न्यायिक रूप से लागू अधिकारों का प्रस्ताव किया
- विद्रोह का अधिकार प्रस्तावित किया — नागरिकों को तानाशाही या निरंकुशता के खिलाफ प्रतिकार करने का अधिकार दिया
मुख्य दृष्टिकोण:
एम.एन. रॉय ने संसदीय संप्रभुता को नकारते हुए नागरिकों को शक्ति का केंद्र माना, न कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को।
➡️ यह नीचे से ऊपर तक लोकतंत्र और राज्य संस्थाओं पर लोगों का प्रत्यक्ष नियंत्रण का विचार अपने समय से बहुत आगे था और आज भी लोकतांत्रिक गहरीकरण पर बहसों में प्रासंगिक है।
दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद: हिन्दुस्तान फ्री स्टेट एक्ट, 1944
1944 में हिंदू महासभा के प्रभाव में तैयार किए गए, हिंदुस्तान मुक्त राज्य अधिनियम ने भारत को एक सांस्कृतिक रूप से एकीकृत और एकात्मक राष्ट्र-राज्य के रूप में देखने की रूपरेखा तैयार की, जिसका शीर्षक था “हिंदुस्तान मुक्त राज्य”। दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद पर आधारित होने के बावजूद, इस दस्तावेज़ में आश्चर्यजनक धर्मनिरपेक्ष गारंटियों के साथ बहुसंख्यकवादी आदर्शों का मिश्रण प्रदर्शित किया गया।
मुख्य बिंदु:
● राष्ट्रीय एकता के लिए “एक भाषा, एक कानून, एक संस्कृति” की वकालत की गई
● किसी भी आधिकारिक राज्य धर्म की घोषणा नहीं की गई और निम्नलिखित का वादा किया गया:
○ धार्मिक स्वतंत्रता
○ धार्मिक आधार पर भेदभाव न करने का वादा किया गया
● मज़बूत केंद्रीकरण का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में प्रांतीय अलगाव की अनुमति देने वाला एक खंड भी शामिल किया गया
● आध्यात्मिक मूल्यों, नागरिक कर्तव्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आपातकालीन शक्तियों पर ज़ोर दिया गया
मुख्य अंतर्दृष्टि:
हालांकि अक्सर इसे बहुसंख्यकवादी या बहिष्कारवादी माना जाता है, लेकिन इस मसौदे में आश्चर्यजनक रूप से उदार-धर्मनिरपेक्ष तत्व शामिल किए गए, जैसे:
● धार्मिक स्वतंत्रता
● कानूनी समानता
● राज्य द्वारा किसी भी धर्म की स्थापना न करने का वादा
यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दक्षिणपंथी संवैधानिक विचारों की जटिलता को दर्शाता है।
विकेंद्रीकृत ग्राम गणराज्य: गांधीवादी संविधान, 1946
श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा महात्मा गांधी की प्रस्तावना के साथ तैयार किया गया, 1946 का गांधीवादी संविधान भारत के भविष्य का एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण एक केंद्रीकृत राज्य के रूप में नहीं, बल्कि स्वायत्त ग्राम गणराज्यों (ग्राम स्वराज) के एक नेटवर्क के रूप में प्रस्तुत करता है। नैतिक और आचार-विचार पर आधारित इस संविधान ने नौकरशाही नियंत्रण पर आत्मनिर्भरता, अहिंसा और विकेंद्रीकरण को प्राथमिकता दी गई है ।
प्रमुख तत्व:
● अहिंसा, ट्रस्टीशिप और ग्रामीण आत्मनिर्भरता पर जोर
● खादी, कृषि और कुटीर उद्योगों को आर्थिक आधार के रूप में बढ़ावा
● न्यूनतम केंद्रीय शासन की वकालत की – जिसमें ग्राम समुदाय अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं करने की बात
● दिलचस्प बात यह है कि इसमें आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार भी शामिल था, जो अहिंसा पर गांधी के सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है
● नैतिक नियमन और नैतिक नेतृत्व के पक्ष में एक मजबूत कानूनी-नौकरशाही राज्य को अस्वीकार
मुख्य अंतर्दृष्टि:
गांधी की संवैधानिक दृष्टि कानूनी प्रवर्तन की तुलना में नैतिक कर्तव्य पर अधिक आधारित थी, जो उनके इस विश्वास को दर्शाती है कि स्वराज (स्वशासन) व्यक्ति और गाँव से शुरू होना चाहिए, न कि ऊपर से नीचे की ओर थोपा जाना चाहिए।
समाजवादी दृष्टि: सोशलिस्ट पार्टी का 1948 का मसौदा संविधान
1948 में, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भारतीय सोशलिस्ट पार्टी ने एक मार्क्सवादी-समाजवादी ढाँचे को दर्शाते हुए एक मसौदा संविधान प्रस्तुत किया। इसने आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय और वर्ग-आधारित लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व पर आधारित एक आमूल-चूल रूप से परिवर्तित भारत की कल्पना की थी – जो पूंजीवादी और औपनिवेशिक दोनों विरासतों को चुनौती देता है।
प्रमुख प्रावधान:
● सभी प्रमुख क्षेत्रों के राष्ट्रीयकरण का आह्वान किया गया:
○ उद्योग
○ बैंक
○ भूमि और प्राकृतिक संसाधन
● उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व समाप्त किया गया
● वर्ग-आधारित विधायिका का प्रस्ताव:
○ प्रतिनिधियों का चयन श्रमिकों, किसानों और बुद्धिजीवियों में से किया जाएगा
● गारंटी:
○ लैंगिक समानता
○ जाति का उन्मूलन
○ पुनर्वितरण और सामाजिक स्वामित्व के माध्यम से आर्थिक लोकतंत्र
मुख्य अंतर्दृष्टि:
वैचारिक रूप से मजबूत होने के बावजूद, मसौदे में संस्थागत तंत्र, प्रशासनिक संरचनाओं और संघीय डिजाइन में स्पष्टता का अभाव था – जिससे यह आदर्शवादी लेकिन संरचनात्मक रूप से अस्पष्ट हो गया।
संविधानिक मसौदों का तुलनात्मक विश्लेषण
| आयाम | 1895 बिल | M.N. Roy का मसौदा | हिन्दुस्तान एक्ट 1944 | गांधीवादी मसौदा 1946 | समाजवादी मसौदा 1948 |
| शासन मॉडल | उदार कानूनीवाद | सहभागी लोकतंत्र | केंद्रीकृत राष्ट्रवाद | ग्राम स्वायत्तता (स्वराज) | समाजवादी केंद्रीय योजना |
| संघीय संरचना | डोमिनियन | भाषाई संघवाद | एकात्मक और पृथक्करण | संघीय ग्राम इकाइयाँ | अस्पष्ट (मजबूत केंद्र) |
| नागरिक स्वतंत्रताएँ | मजबूत नागरिक अधिकार | नागरिक + सामाजिक-आर्थिक | धर्मनिरपेक्ष लेकिन राष्ट्रवादी | नैतिक कर्तव्यों > अधिकार | आर्थिक अधिकार प्राथमिकता |
| आर्थिक दृष्टिकोण | न्यूनतम हस्तक्षेप | लोकतांत्रिक योजना | सीमित आर्थिक सामग्री | कृषिपोषित और गैर-औद्योगिक | पूर्ण राष्ट्रीयकरण |
| संस्कृतिक विचारधारा | ब्रिटिश उदारवाद | धर्मनिरपेक्ष-पंथनिरपेक्ष | एकीकृत हिन्दू संस्कृति | नैतिक एकता और परंपरा | वर्ग एकजुटता |
1950 के संविधान पर इन मसौदों का प्रभाव और धरोहर
ये प्रारूप इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि भारत का संविधान शून्य में नहीं बना, बल्कि प्रारंभिक भारतीय विचारकों और आंदोलनों के बीच समृद्ध वैचारिक बहसों से उभरा है।
निष्कर्ष: संवैधानिक बहुलवाद का प्रमाण
1895 और 1948 के बीच कई संवैधानिक प्रारूपों ने भारत के प्रतिस्पर्द्धी दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित किया – उदारवादी, समाजवादी, गांधीवादी और राष्ट्रवादी। ये दस्तावेज़ केवल आकांक्षापूर्ण नहीं थे – ये भविष्य की संभावनाओं के ब्लूप्रिंट थे, और उन्होंने 1950 के संविधान के अंतिम निर्माण को सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: “1950 के संविधान को अपनाने से पहले, कई संवैधानिक मसौदों में भारतीय लोकतंत्र के विभिन्न मॉडलों की कल्पना की गई थी। इन मसौदों की वैचारिक विविधता और अंतिम संविधान पर उनके प्रभाव पर चर्चा कीजिए।”(250 शब्द)
क्या यह उपयोगी लगा?
संशोधन के लिए बुकमार्क करें, मुख्य परीक्षा के प्रश्न का अभ्यास करें, और
साथी अभ्यर्थियों के साथ साझा करें! धन्यवाद
